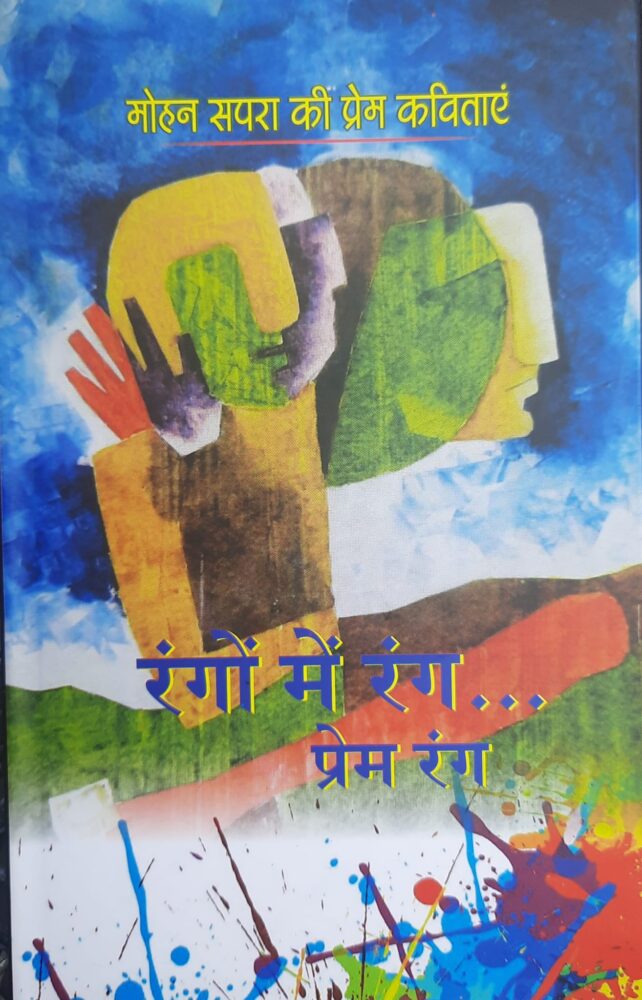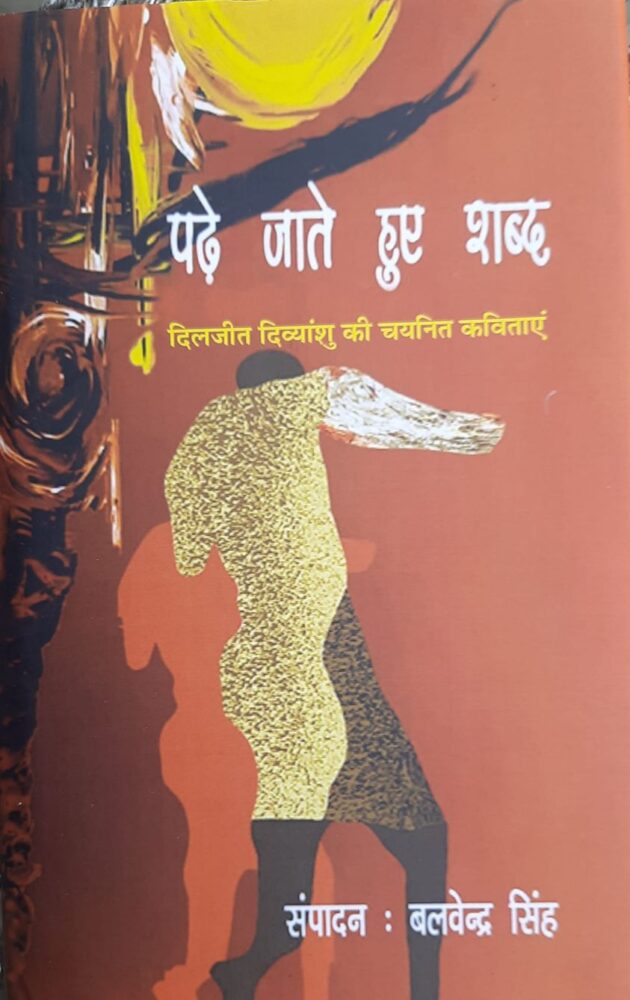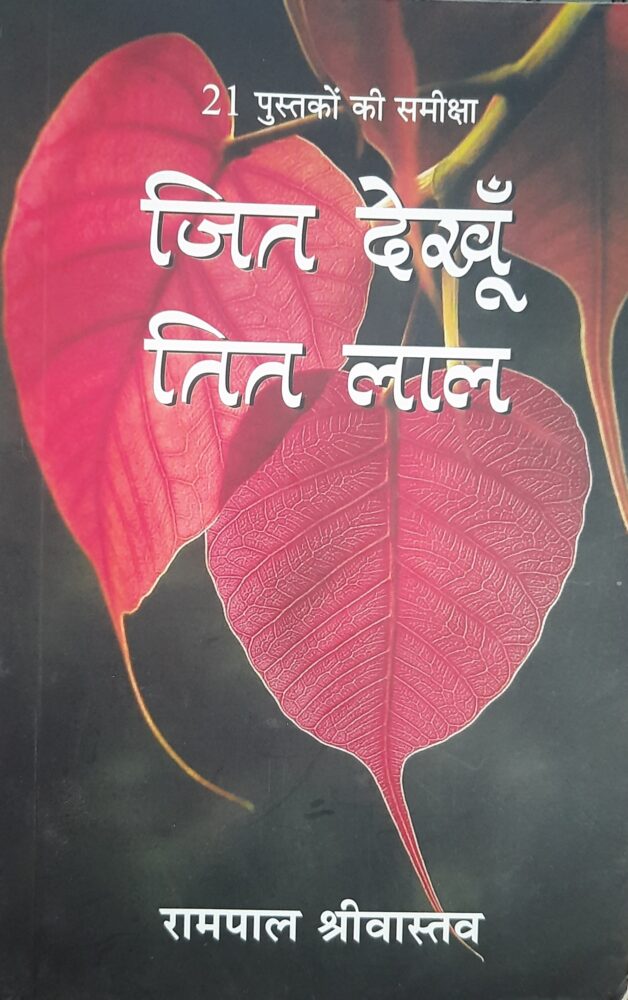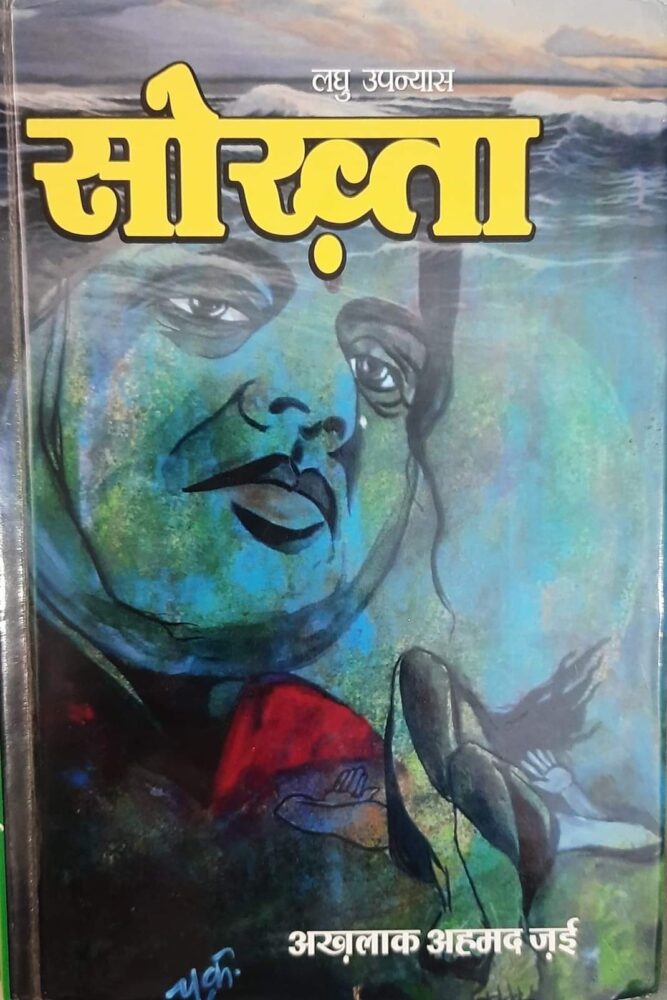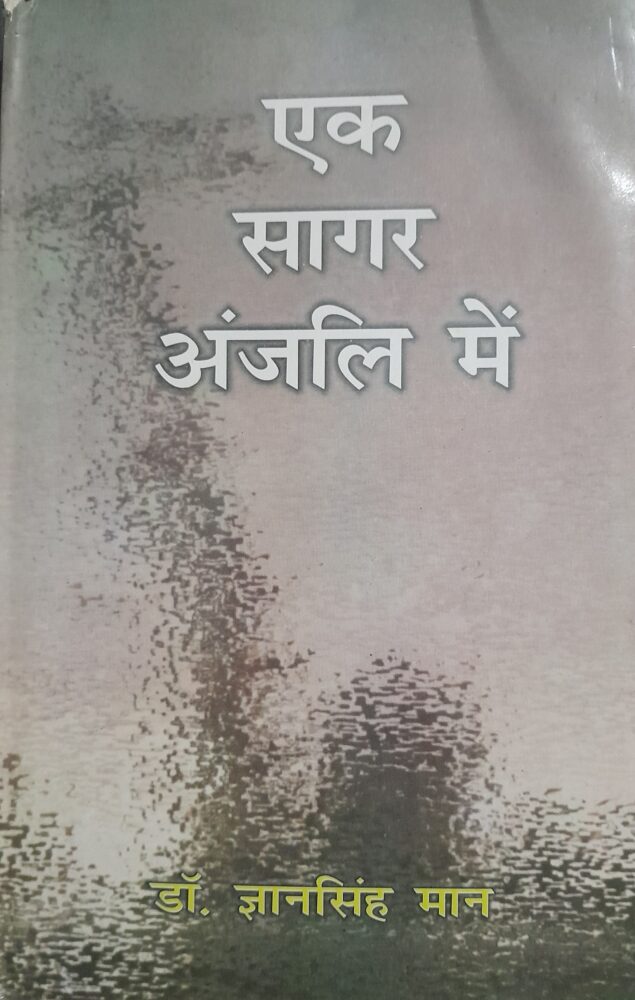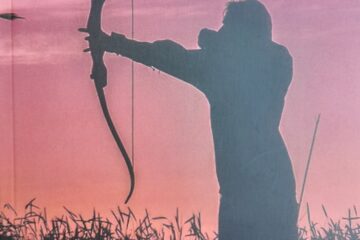जन्म से बालक में जो गुण और संस्कार पाये जाते हैं वे अधिकाँश उसके पिता के गुणों और संस्कारों की प्रतिच्छाया ही होते हैं। बीज और फल में शक्ति, गुण और स्वाद की विशेषतायें प्रायः एक जैसी ही होती हैं। मीठे फल के बीज से उत्पन्न वृक्ष भी मीठे फल ही प्रदान करने वाले होते हैं। वातावरण, जलवायु तथा वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का मत है कि सन्तान के शरीर के न केवल सूक्ष्म गुणों में ही समानता पाई जाती है वरन् स्थूल द्रव्य में भी एकता के सभी लक्षण दिखाई दे जाते हैं।
जीवात्मा के सम्बन्ध में आत्म-विद्या-विशारद आचार्यों का भी यही मत है। वेद, शास्त्र, उपनिषद्, गीता, पुराण, रामायण—इन सब ग्रन्थों में आत्मा के सम्बन्ध में जो विवेचन हुआ है वह एक जैसा ही है। सबने स्वीकार किया है कि जीव अविनाशी तत्व है वह ईश्वर का अंश है। उसमें परमात्मा के सब गुण बीज रूप से विद्यमान है। जीव को अनन्त सुखी, चेतन तथा निर्मल बताया गया है। यह गुण उसके अपने पिता परमात्मा के ही गुण हैं।
किन्तु यदि किसी मनुष्य के जीवन को देखें तो उसमें इन गुणों का अभाव ही दिखाई देता है। आजकल तो विषमता और भी तीव्र हो गई है। सुख की चिर-अभिलाषा रखते हुये भी लोग दुःखी हैं। कष्ट और पीड़ाओं से छटपटा रहे हैं। हर व्यक्ति अशान्त और उद्विग्न ही दिखाई देता है ऐसी स्थिति में कोई भी यह मानने के लिये तैयार न होगा कि प्रस्तुत जीवन में भी ईश्वरीय चेतना का अंश विद्यमान है।
जीव का दूसरा गुण चेतनता, विचार और भावनाओं की शक्ति भी यद्यपि बीज रूप में उनमें देखने को मिलेगी पर यह गुण भी प्रायः किसी में, उपयुक्त मात्रा में, देखने को नहीं मिलता। लोगों में विचार और भावनायें तो उठती हैं पर उनमें अनन्त आकाश को मथ डालने की शक्ति नहीं होती। विचारों की शक्ति किसी से छिपी नहीं है।
विचारों में संसार में भयानक हलचल करने वाली शक्ति है, वैसी ही शक्ति भावनाओं में है। भावनाओं की शक्ति से इस देश में भक्ति के ऐसे सूक्ष्म पर सशक्त स्पन्दन पैदा किये गये हैं—जो इस अधःपतित युग में भी धर्म और संस्कृति को निरन्तर जीवन प्रदान कर रहे हैं। जहाँ इन दोनों गुणों का मेल होता होगा वहाँ की शक्ति का तो कहना ही क्या? जीव में चेतनता का यह गुण बड़ा महत्व रखता है पर वह आज बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है।
जीव के मूल स्वरूप में प्रकट न होने में मुख्य कारण उसमें तीसरे गुण अर्थात् निर्मलता का अभाव है। माया, अविद्या या अज्ञान सब इसी के नाम हैं। मनुष्य को चाहे जिन शब्दों से निन्दित किया जाय पर मुख्य बात एक ही है कि उसने अपने आपको अन्धकारमय, अज्ञानमय अथवा विकारयुक्त कर लिया है इसीलिये वह अपने मूल-स्वरूप को पहचानने में असमर्थ है। गन्दे जल में सूर्य का प्रतिबिम्ब नहीं दिखाई देता, दर्पण मैला हो तो मुखाकृति साफ न दिखाई देगी। जीव मायाग्रस्त, अविद्या या मल ग्रस्त हो तो उसकी भी ऐसी ही दशा होती है। वह अपने ईश्वरीय स्वरूप को पहचानने में असफल ही रहता है।
शाश्वत, मुक्त और अमर जीवात्मा आत्मा ज्ञानता या माया के वश में होकर वैसी ही क्रियायें करता रहता है जैसे बन्दर वाला बन्दर को बाँध कर नचाता रहता है। यद्यपि यह माया कोई दृश्य रूप में नहीं है फिर भी वह लोगों को नचाती रहती है यह कहने की अपेक्षा अब यह कहना अधिक उपयुक्त है कि लोग स्वयं ही अज्ञान में भटक रहे हैं। “हमें क्या करना चाहिए” इस ज्ञान का अभाव ही अविद्या है इसी के कारण लोग गलत कार्य करते और दंड भुगतते हैं।
जिह्वा के स्वाद, नेत्रों की सौंदर्य-लिप्सा, कानों की मधुर संगीत सुनने की इच्छा तथा काम वासना आदि विषयों में आसक्ति हो जाने के कारण विद्या-अविद्या की बात विलुप्त हो गई। जड़ और चेतन में ऐसी गाँठ पड़ गई कि उनका पृथक अस्तित्व भी समझ में न आने लगा।
चेतना ने अपने आपको जड़ मान लिया और जड़ता के काम करने लगे। यद्यपि जड़त्व की, अपने आपको मात्र शरीर मानने की बात नितान्त मिथ्या, भ्रम, अज्ञान है तो भी लोग उसे छोड़ने के लिये तैयार नहीं। युग-युगान्तरों से अभ्यास में आने वाला स्वभाव-गुण एकाएक छूट भी नहीं सकते। जीव ने संसारी होने का अपना विश्वास इतना पुष्ट कर लिया है कि जड़-चेतनता के बीच जो ग्रन्थि पड़ गई है वह छूटती नहीं और जब तक यह भ्रम दूर नहीं होता तब तक कष्ट भी दूर नहीं होते।
महापुरुषों, श्रुतियों, पुराणों ने तरह-तरह के उपाय, अनेक प्रकार के साधन बताये पर जीव के हृदय में साँसारिक सुख, लोभ, मोह आदि का अन्धकार इतना सघन होकर छा गया कि वह इनसे छूटने का प्रयत्न करने की अपेक्षा और भी उलझता गया। मुक्त होने के लिये उसने कुछ प्रयास भी न करना चाहा।
ईश्वर की कृपा या किन्हीं देव-पुरुषों के अनुग्रह से कदाचित इस प्रकार का विचार मन में आ जाय कि आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अपना रहस्य जानना चाहिये, परमात्मा का दर्शन करना चाहिये तो उसे अनेक जन्मों के शुभ संस्कारों का प्रतिफल या ईश्वर की कृपा दृष्टि ही समझनी चाहिये। उस पर यदि किसी के अन्तः करण में श्रद्धा जागृत हो जाय तो उसे अपना बड़ा सौभाग्य मानना चाहिये।
श्रद्धा का उदय होना निश्चय ही अनेक जन्मों के पुण्यों का प्रतीक है पर अकेली श्रद्धा ही आत्म-कल्याण नहीं कर देती वह तो अपने जीवन लक्ष्य की ओर उन्मुख करने वाला प्रकाश मात्र है। उनको यात्रा पथ पर चलने की भी आवश्यकता है। शास्त्र इस क्रिया को धर्माचरण बताते हैं। अर्थात् श्रद्धा उदय हो तो मनुष्य को जप, तप, व्रत, यम, नियम आदि साधनों का आश्रय लेकर जीवन और आत्म-शोधन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर देनी चाहिये। संसार में जितने भी कर्म हैं वे सब धर्म का आचरण कहलाते हैं इनसे आत्मा का बल बढ़ता है और उसमें निर्मलता आने लगती है।
आत्म-कल्याण की साधनायें भावनाओं का रस पाकर शीघ्र फलदायिनी होती हैं यों इन साधनाओं में उदासीनता हो तो भी प्रगति तो होती ही है किन्तु जब भावनाओं का सम्मिश्रण हो जाता है तो साधना से ही एक अलौकिक आनंद की रसानुभूति होने लगती है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो समय की दूरी थी वह कम अखरने लगती है। भावना मनुष्य की साधना में सफलता की आशंका को भी कम कर देती है। “मैं तेरा हूँ अब तुझे छोड़कर कहाँ जाऊँ।
मुझे अज्ञान से निकाल और मानव-जीवन के उपयुक्त आचरण करने की क्षमता प्रदान कर। अब मेरे जीवन का सर्वस्व तू ही है।” इस प्रकार की भावनायें आत्म-कल्याण के पथिक को बड़ा बल प्रदान करती है। विश्वास बढ़ाती हैं और मन में चढ़े कुसंस्कारों के ढेर को बात की बात में जला कर खाक कर डालती हैं। साधना काल में भावनाओं का होना इसी दृष्टि से बड़ा शुभ और लाभजनक माना जाता है। भावनायें जिसे मिल जायँ उसे अपने आप पर ईश्वरीय विशेष कृपा ही माननी चाहिए।
इस प्रकार भक्त धर्म-कर्म करते हुये मन की कामनाओं को मारता और उसे काम, क्रोध, लोभ मोह, छल, द्वेष, पाखण्ड, झूठ, बेईमानी आदि दुष्प्रवृत्तियों से विमुक्त करता है। वासनायें और साँसारिक प्रलोभन उसे बार-बार अपनी ओर आकर्षित करते हैं वह बार-बार इनसे लड़ता है, इन्हें मारता है, आत्मा के गुणों को बढ़ाता है।
दया, क्षमा, करुणा, सन्तोष, समता, धृति आदि सत्गुणों का विकास करता है। इंद्रियों का दमन करता है और जो दोष-दुर्गुण होते हैं उन्हें बार-बार ठीक करता है, सत्य प्रवृत्तियों की शोध और दुष्प्रवृत्तियों के विरोध का विचार कभी भी मन्द नहीं होने देता वरन् वैसा करते हुये वह उत्साह अनुभव करता है। विचार-मन्थन के द्वारा वह सत्य को आग्रहपूर्वक अपने जीवन में धारण करता और दुष्कर्मों, असत् तत्वों का परित्याग करता जाता है।
यह विज्ञानमय बुद्धि अन्तः करण की ममता, मद, मोह आदि को जला डालती है उस अवस्था में केवल ब्रह्म की अखण्ड और दिव्य-ज्योति आत्मा में ही अनुभव होने लगती है। यह प्रकाश मनुष्य के अज्ञान, अविद्या या माया को भस्म कर डालता है मनुष्य जीव-भाव से मुक्त होकर पुनः अपने परमपिता-परमात्मा की गोद में ही समा जाता है यह अवस्था अनन्त सुख,अनन्त आनन्द की अवस्था होती है।
– पंडित कृष्ण दत्त शर्मा