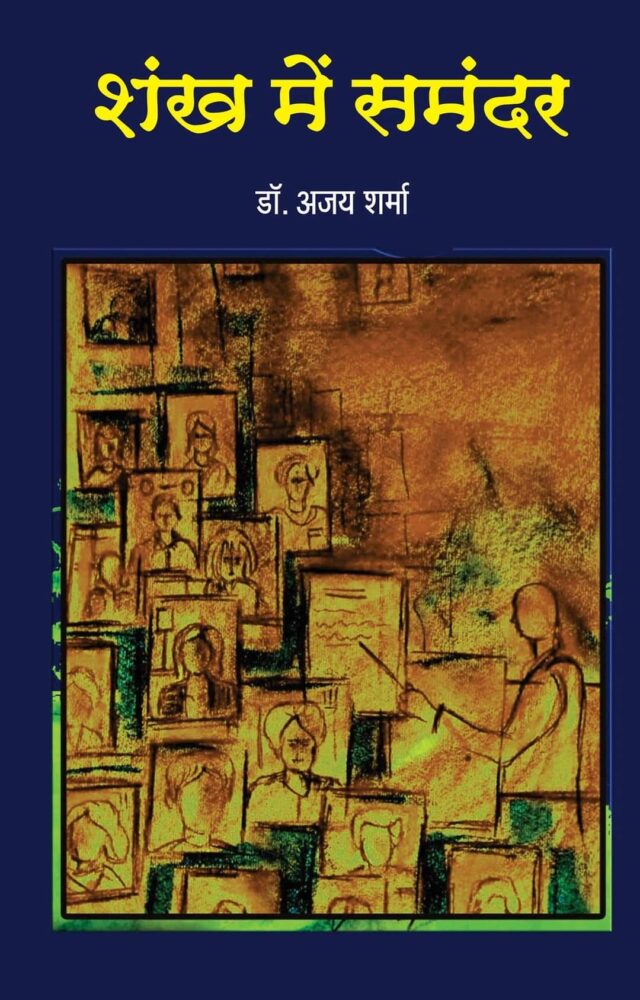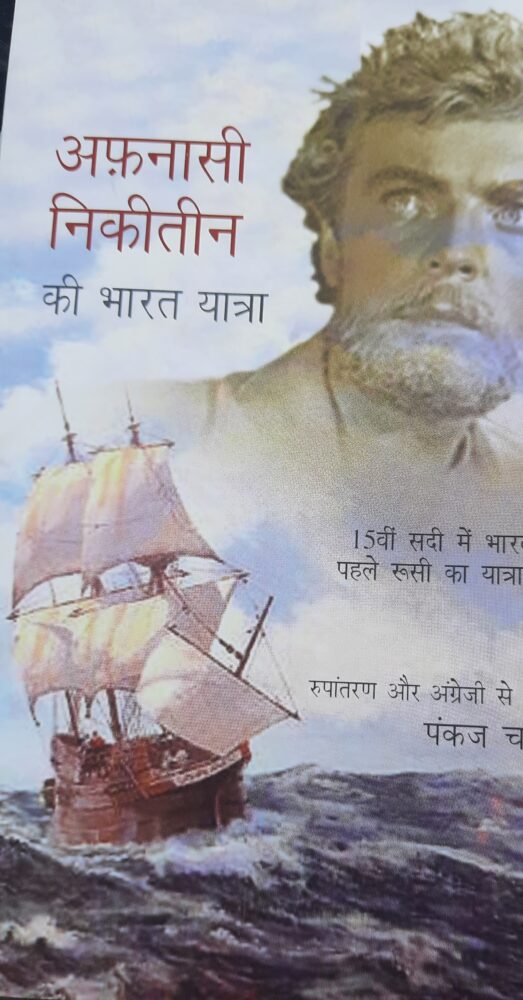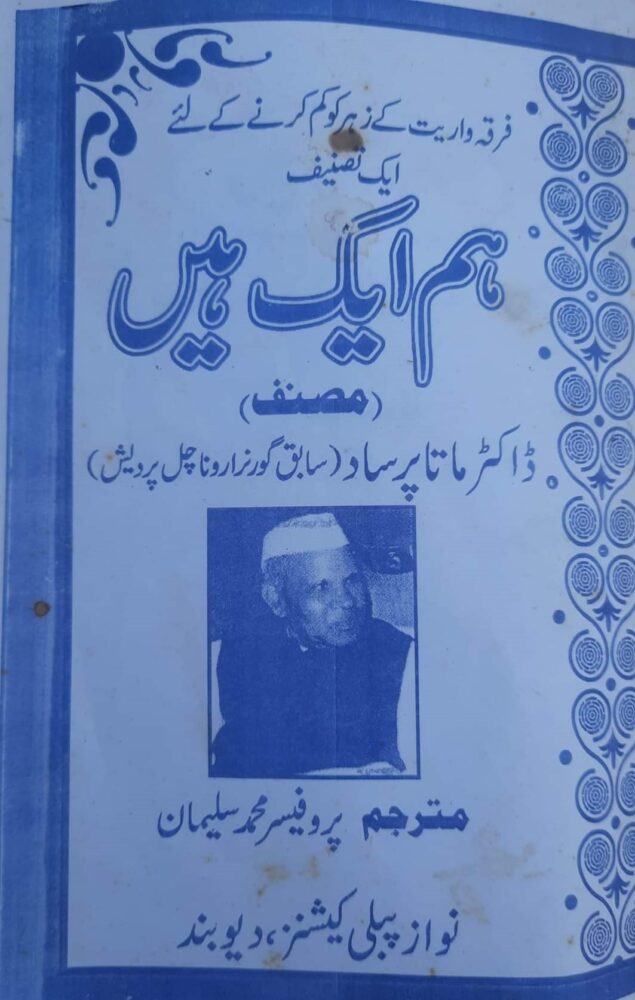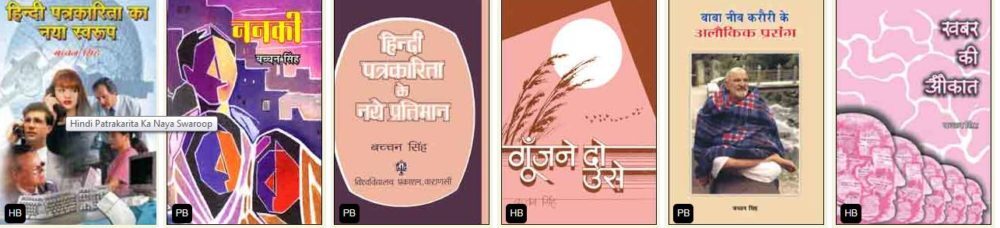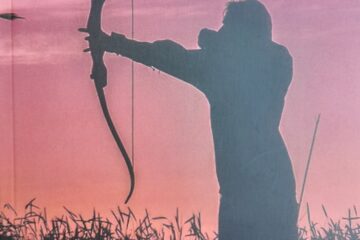लगभग 35 वर्ष पहले जब मैं कोलकाता गया था बीबीसी के एक चुनावी कवरेज ( सर्वे ) का हिस्सा बनने, तब तक यह महाशहर अपने असली वजूद में था। उस वक्त कहा जाता था कि जिसने हाथ रिक्शा नहीं देखा और उस पर सवारी नहीं की, उसने कोलकाता का असली रूप नहीं देखा,उसका मर्म नहीं समझने की कोशिश की। दिल से कहूं तो… वैसे मैं दिल से ही अधिक काम करता हूं …
मैं जब इस हाथ रिक्शा पर बैठा, तो अपने को अपमानित महसूस किया। मन में इस आशय के विचार उठने लगे कि शायद मैंने कोई अपराध कर डाला हो इसकी सवारी करके … एक इंसान को एक इंसान पेट की खातिर अपने सीने पर जुआ रखकर खींच रहा है! यह मेरे दिल को दुखा गया। मैंने फ़ौरन इससे उतरने का इरादा कर लिया। रिक्शावाले भाई से कहा, ” भैया, रुको। बस यहीं छोड़ दो। अब आगे नहीं जाना। ” भाई का चेहरा कुछ फीका पड़ गया। जहां – तहां चिंता की लकीरें खिंच गईं। मैं समझ गया कि रिक्शेवाले भाई की मानसिक स्थिति। मैंने कहा, ” लेकिन आपको मैं पूरे पैसे दूंगा। ” भाई बोल पड़े, ” बाबू मोशाय, सोमस्या नेई। ( बाबू साहब, कोई बात नहीं )
मैंने उनको तय रकम से काफ़ी अधिक पचास रूपए देने लगा, जिसे लेने से उन्होंने इन्कार कर दिया , तो मैंने यह कहते हुए कि ” ले लीजिए मेरी ओर से बच्चों के लिए टॉफियां लेते जाइएगा ” उनकी जेब में डाल दिया। वे बहुत खुश हो गए। चेहरे पर प्रफुल्लता का भाव साफ़ दिखा।
मेहनत अधिक मेहनताना मामूली, यह सदियों का दर्द रहा हाथ रिक्शा चालकों का, लेकिन लंबे अरसे तक किसी ने उनके दर्द को महसूस नहीं किया । हुआ बस इतना कि चुनावों के समय उनके गिरते आंसुओं को पोछने की दिलासा ज़रूर दिलाई जाती, लेकिन चुनाव बाद उनके हितार्थ होता कुछ नहीं ! विडंबना यह भी कि शासन भी उन्हीं पार्टियों का मुद्दतों तक रहा, जो रात – दिन मज़दूर हित का रोना रोते रहते हैं। यह प्रथा बार – बार इंसान को सामंती युग में ले जाती थी, जिसके विरोध में वामपंथ का जन्म हुआ। मगर यहां तो अपनी ही चलानी थी, अंथ – पंथ से क्या मतलब !! ज्योति बसु तवील अरसे तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे, मगर हाथ रिक्शा वालों की समस्याएं बनी ही रहीं। पिछले कुछ वर्षों से सरकारी प्रयासों से इस पर रोक लग गई है। ममता बनर्जी ने इस ओर जो गंभीरता दिखाई , वह सराहनीय है।
हाथ से रिक्शा खींचने का चलन यहां बहुत पुराना था। बंगला भाषा में इसे ” ताना रिक्शा ” नाम दिया गया था…. अलविदा ताना रिक्शा !!!
ताना रिक्शा 1869 ई. में आविष्कृत हुआ और 1874 में चीन में पेश किया गया। फिर यह इन देशों के साथ सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत में फैला। भारत में इसे अंग्रेज़ लेकर आए। इसलिए भी इसे औपनिवेशिक अवशेष माना और लिखा जाता रहा है। अंग्रेज़ो
के भारत छोड़ने के उपरांत भी यह रिक्शा कोलकाता की धरती पर जीवंत रहा !
विश्व साहित्य जगत सबसे पहले ताना रिक्शा पर चीन में साहित्य रचा गया। पूरा उपन्यास ही लिख डाला मूर्धन्य उपन्यासकार लाओ श ( Lao She – 1899- 1966 ) ने ” रिक्शावाला ” लिखकर। वे इस रिक्शा के चलन से अत्यंत मर्माहत हैं। उपन्यास में ख़ुद को ही पात्र बना लेते हैं।
इस उपन्यास में खुद को ही पात्र बना डालते हैं। ” रिक्शावाला ” उपन्यास में लाओ श गांव से जैसे ही शहर आता है, उसकी बर्बादी की दास्तान शुरू हो जाती है। वह बहुत मेहनती रिक्शावाला है, किंतु अभावग्रस्त है। बहुत मेहनत करने के बाद अंटता नहीं था, फारिगुलबाली और सम्पन्नता कोसों दूर थी। उसके पड़ोसी भी गरीब थे। छोटे – मोटे कामों में लगे रहते थे। सबका जीवन अभावों में था। लाओ श पर परिवार के भरण – पोषण की ज़िम्मेदारी थी। वह विद्यालय नहीं गया, इसलिए अधिक विकल्प नहीं थे रोज़ी के उसके पास। रिक्शा पर उसका हाथ बैठा हुआ था। संघर्षों में ही उसका जीवन बीत जाता है। कुछ हासिल नहीं कर पाता। दूसरा प्रमुख पात्र श्यांगचि का जीवन भी बहुत कष्टप्रद है। बहुसर्जक आधुनिक लेखक लाओ श चाहता है कि यह प्रथा मिटे, जो आदमी, आदमी को सीने पर ढोए उस परिपाटी का अंत हो। भारत में हिंदी में असगर वजाहत ने ” दो पहियोंवाले रिक्शे ” ( उपन्यास ) में ऐसे रिक्शावालों की दुर्दशा का चित्रण किया है।
– Dr RP Srivastava
Chief Editor, Bharatiya Sanvad