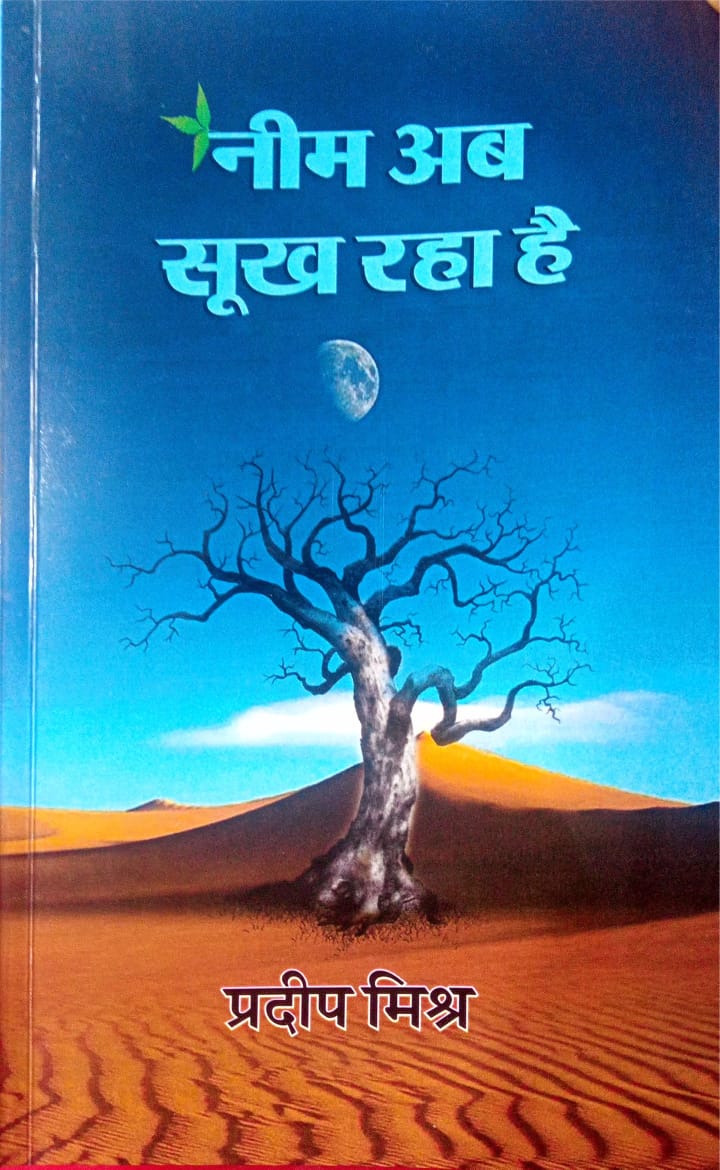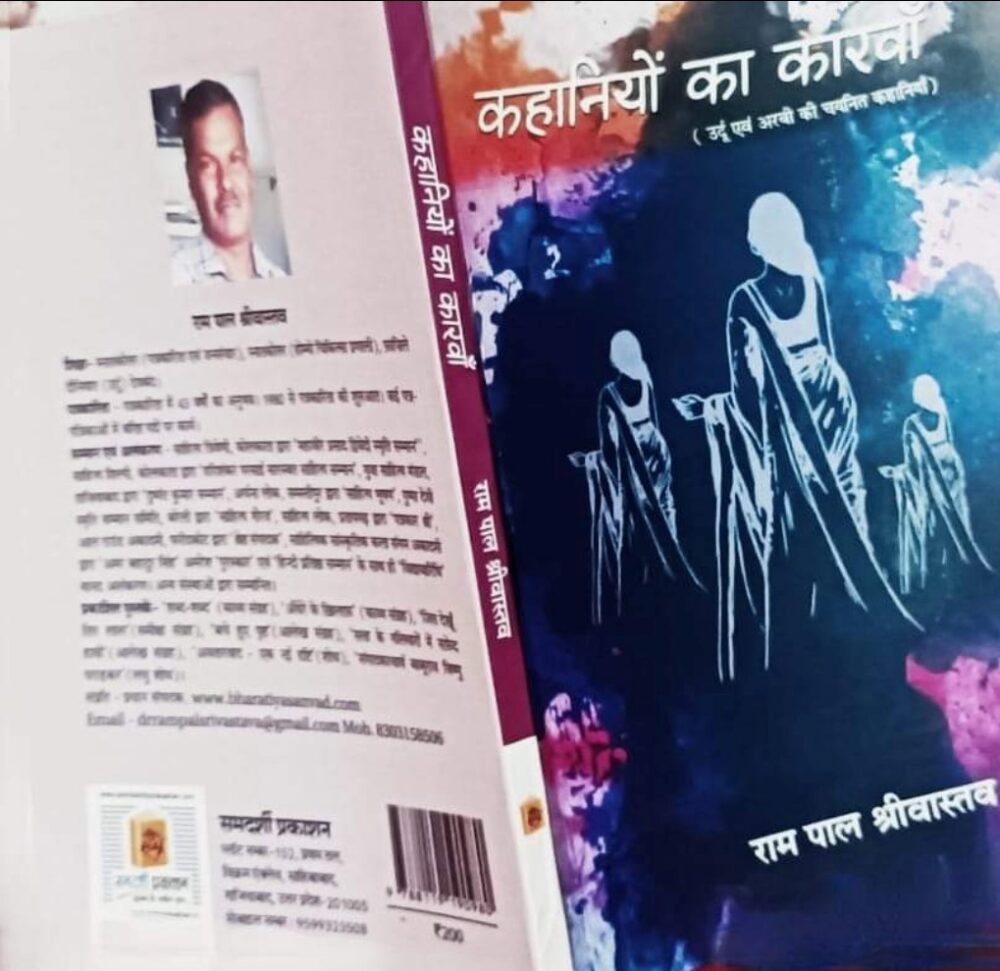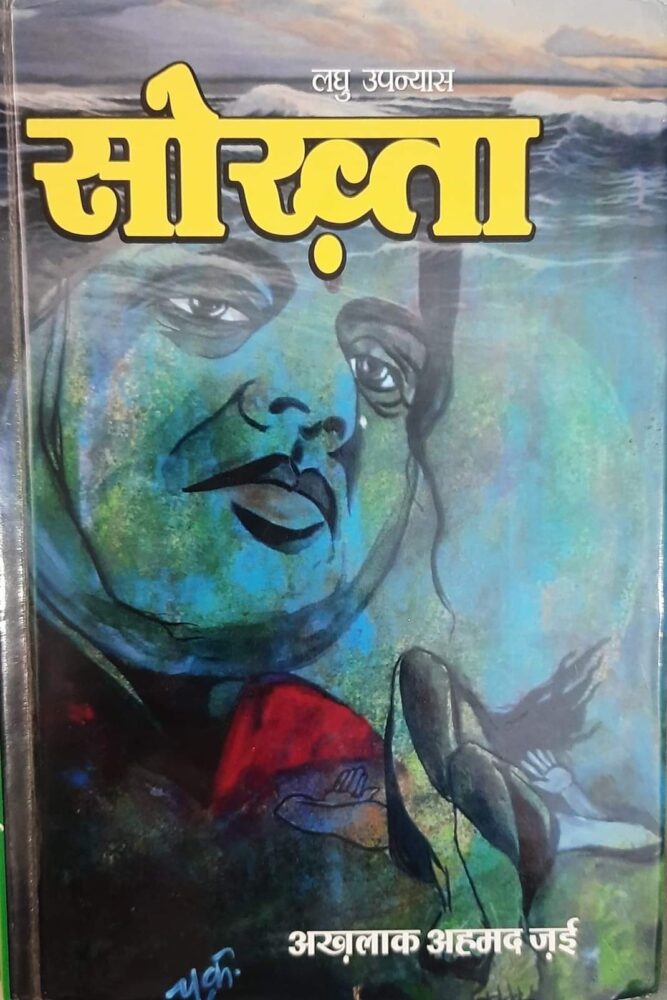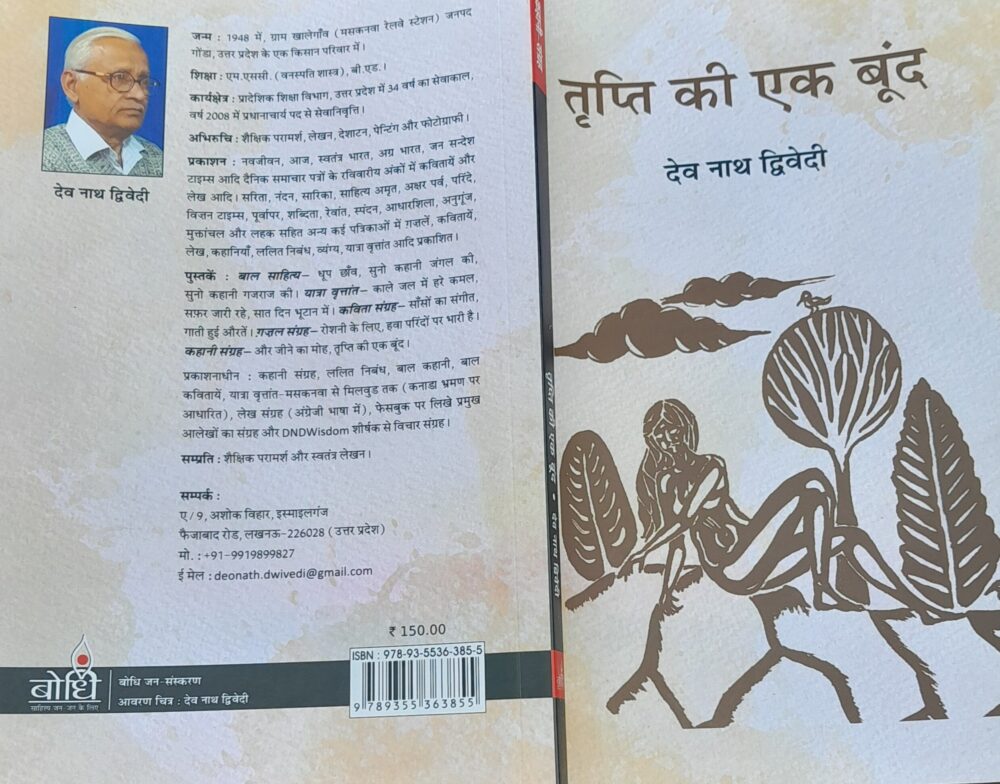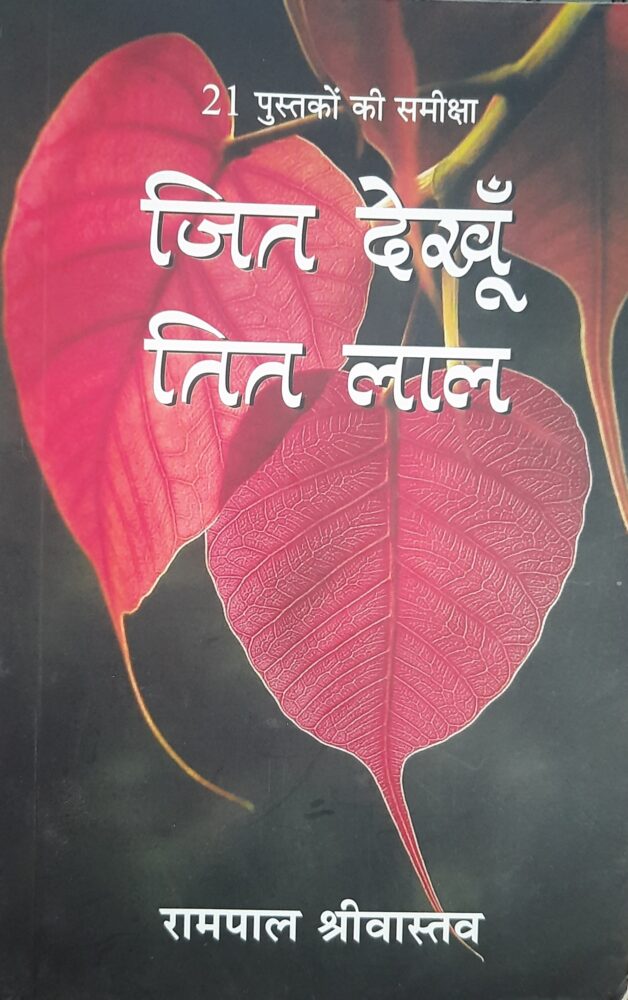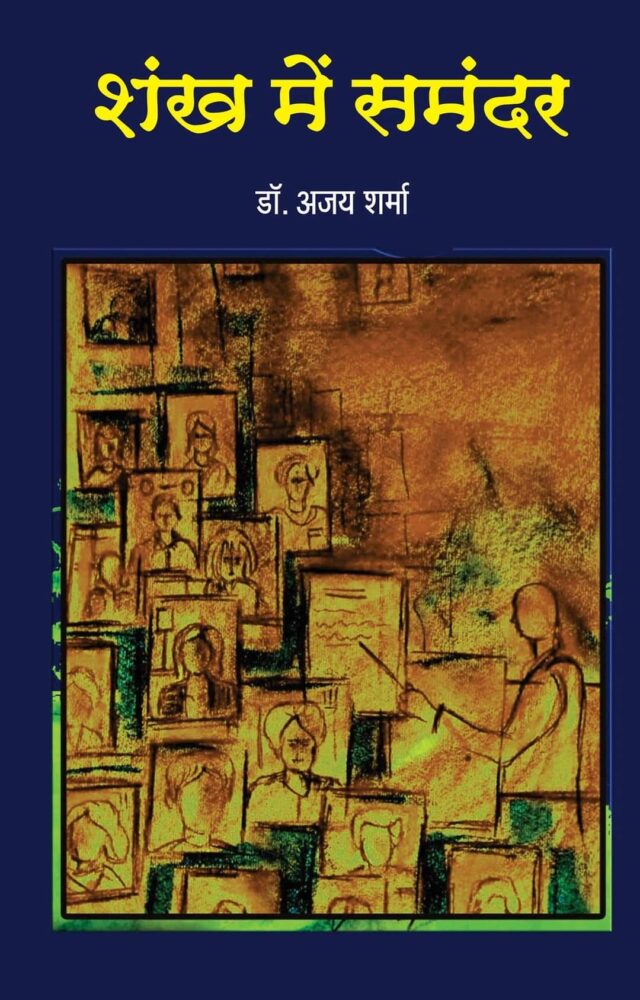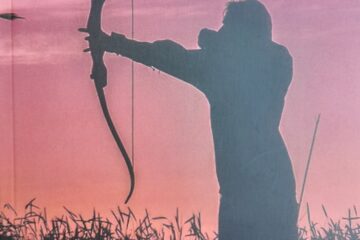” नीम अब सूख रहा है ” क्योंकि उसकी छांह के नीचे उसी की छांह को खरीदने – बेचने का जो सिलसिला चल रहा था, उसका आख़िरी नतीजा आ चुका है। पतन के दौर में जिस आदर्श और मूल्य की तलाश कभी हरफ़नमौला रचनाकार राही मासूम रज़ा ने पूरे मन से की थी ” नीम का पेड़ ” ( उपन्यास ) लिखकर, उसी तलाश को आगे बढ़ा रहे हैं प्रतिभावान कथाकार प्रदीप मिश्र। उनका कहानी संग्रह ” नीम अब सूख चुका है ” इसी तलाश की एक मज़बूत कड़ी है। समाज से लोप होते जीवन मूल्य कैसे बचें और फिर से लहलहाएं, इसकी ही अव्वल चिंता कथाकार को है। उसे नंद लाल भारती की भांति आशंका नहीं कि उसकी कोशिश बेकार हो जाएगी और उसके नीम के अधिकतर पौधों को बकरियां चर लेंगी। ” नीम का पेड़ ” ( कहानी ) में नंद लाल भारती एक पौधे को बचा पाते हैं, जबकि परिवार की पहचान करार देकर राधा किसन मूंदड़ा नीम के पेड़ को काटने से रोकने में जी जान लगा देते हैं। ( ” नीम का पेड़ ” कहानी )
इन सबसे आगे बढ़कर प्रदीप मिश्र समग्रता में विश्वास रखते हैं और अपनी कहानियों में जीवन – आदर्श, मूल्य और संस्कार को पूरे तौर पर अंगीकार करने की सफल वकालत करते हैं। उनका मानना है कि ये सब हमारे अतीत के गौरव हैं, जिनको अपनाने से ही जीवन सार्थक हो सकता है। ” नीम अब सूख रहा है ” उनका पहला कथा – संग्रह है, जिसमें कुल पंद्रह कहानियां हैं, जिनमें से एक को छोड़कर सभी पूर्व में विभिन्न पत्र – पत्रिकाओं में विभिन्न काल क्रमों में प्रकाशित हुई थीं। इसकी पहली कहानी से पुस्तक का शीर्षक निर्मित है। हिन्दी में कहानियों की शुरुआत भले ही बांग्ला और अंग्रेज़ी के अनुकरण रूप में हुई हो, कुछ अनूदित हों, लेकिन शीघ्र ही ये अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में कामयाब हुईं।
प्रदीप मिश्र की सभी कहानियां पूर्णतः यथार्थवादी हैं, जिनमें पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक चरित्र – चित्रण है। इनमें सामाजिक सरोकार के बदलते आयाम हैं। सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों और भ्रष्ट आचरण पर फोकस है, फिर कहानियों की घटनाओं का क्रम अधिक जटिल नहीं है।
सभी कहानियां एक विशेष प्रकार की संवेदना जगाती हैं, जिससे उनका अंतिम दृश्य देखने की उत्कंठा पैदा हो जाती है। ऐसे में जिसने भी कहानी पढ़नी शुरू की, प्रायः वह अंत तक पढ़े बगैर नहीं रहता।
कहानियों में सरलता, प्रवाहमयता, स्वाभाविकता और मुग्धकारिता के गुण खुले रूप में विद्यमान हैं। ये सभी प्रायः उत्तम पुरुष वाचक और पात्र – प्रधान हैं। ये पांडेय बेचने शर्मा ” उग्र ” की कहानियों की सिमलरटी लिए हुए हैं, जिनमें आदर्शवाद का खुलकर सम्मिश्रण नहीं किया गया है प्रेमचंद की तरह। प्रदीप मिश्र पूर्णतः यथार्थवादी हैं ” उग्र ” की तरह। फिर भी उनकी कहानियों में राधाकृष्ण और फणीश्वर नाथ रेणु की तर्ज़ पर कथाक्रम कभी तेज़ी से चल पड़ते हैं। चलिए प्रदीप मिश्र को पहले के दौर का पांडेय बेचन शर्मा ” उग्र ” और बाद के दौर के यादवेंद्र शर्मा ” चंद्र ” जैसा यह मान कर मान लेते हैं कि कोई किसी का बदल नहीं हो सकता !
प्रदीप मिश्र की कहानियों में अवधी भाषा की चाशनी देखते ही बनती है। इन शब्दों की गुणवत्ता देव – प्रसाद के आस्वादन सदृश है।
” नीम अब सूख रहा है ” में कुल पंद्रह कहानियां हैं। सभी की अपनी इनफिरादी हैसियत है। सभी की अपनी विशिष्टता है। पहली कहानी जो पुस्तक का शीर्षक ही है,आंचलिक है। कस्बाई कहानियां भी हैं और इन दोनों धरातलों के मिलेजुले संयुक्त वातावरण वाली भी हैं। ये कहानियां विभिन्न पत्र – पत्रिकाओं में पूर्व प्रकाशित है, “पंडित जी” को छोड़कर।
नीम प्रतीक है गांव की मर्यादा, परंपरा और आदर्श का। इस पर बया का बसेरा है, जिन्हें सांप से एक बार तो बचा लिया जाता है, लेकिन दूसरी बार सांप उन्हें बेदखल करने में कामयाब हो जाता है। उस तक गांववासी नहीं पहुंच पाते। नए भ्रष्ट प्रधान ने उसे अवैध रूप से अपने अहाते में जो ले रखा है। गांव के लोग चाहरदीवारी को लांघकर बया पक्षियों को बचाने का साहस न कर सके। सांप को मौक़ा मिल गया लोगों की मानसिकता को विषाक्त करने का । और इस प्रकार लोग विभिन्न विकारों में फंस गए। नीम सूख गया। नैतिकता मर गई। इस प्रकार यह कहानी अपने अद्देश्य में सफल हो जाती है। इसमें कथाकार कुछ सार्थक संवाद भी करता है, यथा –
” काश ! हमारी कायर सरकार भी पाकिस्तानी आतंकवादियों से भी ऐसी ही सख्ती से निपटती, तो देश से आतंक कब का खत्म हो गया होता …।” ( पृष्ठ 19 )
( ग्राम प्रधान के प्रति ) ” सिर से पांव तक स्वार्थ में डूबा इन्सान भला कैसे समझ सकता है एक पेड़ होने का अर्थ? दूसरों के लिए जीने का मतलब ?” ( पृष्ठ 23 )
” वैसे ये तो सियासत का अघोषित नियम ही है कि इसका लाभ बस चंद लोग ही उठाते हैं, लेकिन इसकी असली क़ीमत सिर्फ़ मासूम – निर्दोष ही चुकाते हैं।” ( पृष्ठ 23 )
कहानी में अवधी के संवाद इसकी शोभा बढ़ा देते हैं। दो बातें कुछ अटपटी और अतिरंजित लगीं – रामबली पहलवान का अस्सी फुट की गहराई में कुएं में उतरना और सांप का कई सप्ताह तक मौत का तांडव। कुआं इतना गहरा अपवाद ही है और सांप की आदत लंबे समय तक शिकार की नहीं होती।
‘ भूख ‘ शीर्षक कहानी समाज की सीधी अक्कासी करती है, जो हक़ीक़त पर आधारित अधिक लगती है। अगर ऐसी न होती, तो शायद ही पुरस्कृत होती। वैसे किसी भी समाज में हर जगह एक जैसी परिस्थितियां नहीं होती। कभी ये परिस्थितियां बोलियां सदृश हो जाती हैं, जो कोस दस कोस पर बदल जाती हैं। कोई। ही यह नहीं कह सकता कि अमुक समाज में व्यवहार में एक ही परिपाटी और स्थितियां होती हैं। अपवाद की बात अलग है।
‘भूख ‘ में नसरीन बी की ज़िंदगी पर आधारित व्यथा – कथा के जो आयाम हैं, वे कृत्रिम व असहज नहीं लगते। सच है कि धर्मनेताओं का समाज पर विभिन्न रूपों में दबाव रहता है। यह बात ज़रूर है कि इसमें न्यूनता – आधिकता और कद के हिसाब से वर्चस्व का अंतर भी रह सकता है। देखा गया है कि धर्मनेताओं की भृकुटी तनी, तो सभी चित हो जाते हैं। नसरीन बी में कहां इतना दम कि वे इस भारी भरकम बाहरी दबाव को झेल लें। बड़े – बड़े तो झेल ही नहीं पाते।
परिस्थितियों की मारी नसरीन बी की भूख इतनी भरी हुई थी कि ज़कात और सदक़ात उनके कुछ काम नहीं आ पा रहे थे। ज़कात मदरसे चट कर जाते और सदकात अपने ख़ास लोग। वह अगर आस्तानों का तबर्रूक ले लेती तो चलता, मगर दबाव वालों को प्रसाद हज़म नहीं हुआ। फिर भूखे पेट में अन्न चला गया तो कुफ़्र तो नहीं टूट पड़ा।
हदीस में है, ” ऊपर वाला हाथ ( अर्थात देनेवाला) नीचे वाले हाथ से अच्छा है( बुखारी, मुस्लिम)। मगर देता कौन है ? जिसने भी दिया उसका हाथ ऊपर हुआ, जिसकी तारीफ़ होनी चाहिए। साहिबे निसाब देते तो समाज की वह दुर्गति न होती जो नसरीन की हुई। नसरीन बिला वजह हाथ भी नहीं फैलाती, इसलिए उसकी भूख का मुबालग़ा लगाना नजायज है। ऐसे में नसरीन को जगह बदर के लिए मजबूर होना लाज़िमी बात थी। हर कहानी में कुछ न कुछ उड़ान ज़रूर होती है , वरना वह कहानी ही न हो |
जिस धर्म में जान बचाने के लिए अविहित को भी खाने/ कहने की गुंजाइश हो, वहां का ऐसा वातावरण सर्वथा निन्दनीय है। यह कट्टरता की निशानी है और यह ‘मन तशब -बहा…..’ में नहीं आता । वैसे भूखे को खाना खिलाने के एवज़ में ख़ुदा को पा जाना (हदीसे क़ुदसी ) अच्छा है।
‘भूख ‘ को धार्मिक चश्मे से देखना गलत है। धर्म के कथित ठेकेदार जो कहते हैं, ज़रूरी नहीं कि धर्म के एकदम अनुरूप हो । इसीलिए वे ठेकेदार बन जाते हैं।
भूख के कथ्य बड़े ज़ोरदार हैं। शिल्प उत्कृष्ट कहानी के पैटर्न पर है और कथानक ग़ज़ब का है। इस कहानी का यथार्थ धरातल है, जिस पर नाना प्रकार के पुष्प खिले हैं। निश्चय ही यह हमारे गौरवशाली देश का धरातल है, जहां सहिष्णुता की अविरल धारा सदियों से प्रवहमान है, जो हर संकीर्णता और कट्टरपन को तोड़ती रहती है।
” लालच ” में मेडिकल भ्रष्टाचार का पर्दाफाश है। सजीव चित्रण है डाक्टर की धनलोलुपता का और रोगी की दयनीयता का। अब डॉक्टर भगवान रूप नहीं रहे। येन केन प्रकारेण धन दोहन के यंत्र बन चुके हैं। सचाई यह है कि आज की बहुतेरी मेडिकल संस्थाएं मानव – वध की अघोषित केंद्र बन गई हैं और इन्हें यह सब करने का सरकारी लाइसेंस मिला हुआ है ! ” लालच ” पढ़कर डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी की याद आई, जिन्होंने मेडिकल भ्रष्टाचार पर भारत की पहली पुस्तक लिखी और नतीजे में विरोधों का डटकर सामना किया। इस पुस्तक का नाम है, ” हॉस्पिटल से ज़िंदा कैसे लौटें ?” इसमें स्वास्थ्य उद्योग के सच का बयान है। अस्पताल फांसी का फंदा कैसे हैं, सोदाहरण समझाया गया है। अतः ऐसे उद्योग को हतोत्साहित करने की ज़रूरत है। दूसरी ओर इसकी उपादेयता से इन्कार नहीं, इसकी व्यावसायिकता और नृशंसता की मानसिकता का इन्कार है। इस कहानी में एक असावधानी है, वह यह कि नर्सिंग होम में अमूमन लीवर सिरोसिस का इलाज नहीं होता ! कथाकार को अस्पताल या क्लीनिक लिखना चाहिए और उसी में कथाक्रम फिट करना चाहिए।
ग्राम प्रधान के भ्रष्ट आचरण को ” मुआवज़ा ” में उजागर किया गया है। आंचलिक कहानी है यह पुस्तक के शीर्षक वाली कहानी की भांति। पंचे की मौत के बाद वह कमली को मुआवज़ा दिलवाता है और डेढ़ लाख में से पचास हज़ार पा जाता है। ग्रामीण जीवन की व्यथा को दर्शाने में सफल है कथाकार। इसमें पृष्ठ 36 पर एक सहज भूल देखने को मिली, वह यह कि कथाकार ने लिखा है, ” …उन नर्तकियों ने गुलाम अली की एक मशहूर ग़ज़ल पर भी हाथ साफ़ कर हैरत में डाल दिया था … हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफ़िर की तरह …” यह ग़ज़ल कैसरुल जाफरी की है, जिसको गुलाम अली समेत दर्जनों गायकों ने सुर दिया है। कहानी में अवधी भाषा के वाक्य कहानी में चार चांद लगा देते हैं।
” आखिरी आस ” सामाजिक तानेबाने पर बुनी कथा है। प्रत्येक मनुष्य को जीवन के अंतिम भाग में किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। घर का सदस्य सहारा बने , तो अति उत्तम। बेटे नरेंद्र की दंगे में मृत्यु हो जाती है, बहू पर मायके चली जाती है। वह गर्भवती थी। बेटे को जन्म देती है, जो अपने बाबा के अंतिम जीवन में सहारे की आस बनता है। यह कहानी अधिक मनोवैज्ञानिक है। इसका यह वाक्य उल्लेखनीय है, ” बाप के प्रेम की लहरें बचपन की प्यासी ज़मीन को भिगो तो सकती हैं, लेकिन उसकी प्यास तो बस ममता की धार से ही बुझती है।”( पृष्ठ 46)
” पंडित जी ” भी मनोवैज्ञानिक कहानी है, जिसमें पंडित जी की स्वार्थपरक मानसिकता को उकेरा गया है। बदले परिवेश में भी अपनी कार्यशैली को थोड़ा चेंज कर भी वे अपनी मनोवृत्ति नहीं बदल सके अधिक से अधिक धन संग्रहण की। नैतिकता नष्ट – भ्रष्ट हो, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं ! उनका परम सहयोगी है रामू नाई। साथ – साथ साए की तरह लगा रहता है। आरती के पैसे पा जाता है। इतने में संतुष्ट रहता है, जबकि उसके दो लड़के हैं, परिवार है।
समर प्रताप मंत्री के यहां भागवत कथा में रामू को महसूस हुआ कि पंडित जी का व्यवहार उसके प्रति रूखा हो गया है। कारण वह समझ नहीं पा रहा था… पंडित जी मंत्री जी के सेवाभाव, आवभगत और दान – दक्षिणा से काफ़ी प्रसन्न हुए। अंतिम दिन ऊंची व्यास गद्दी पर बैठे। वे आश्चर्य मिश्रित चिंता में डूब गए। ” रामू को मिलनेवाली आरती की धनराशि उन्हें आज बहुत अखरने लगी थी।” अतः जब रामू आरती की थाल पकड़ने चला, तपाक से पंडित जी बोल पड़े, ” रामू , आरती की थाल तुम छू नहीं सकते।” पंडित जी ने पूछा, ” तूने स्नान किया है आज।” फिर पंडित जी ने “आरती की थाल अपने कमीशनवाले पंडित की ओर बढ़ा दी।” रामू तिरस्कार की आग में धू – धू कर जलता रहा। उसने अपने घर की राह पकड़ ली। इस कथा में स्वार्थ, विश्वासघात, लालच, शोषण और ढोंग खेलकर दिखा। यह अपने मंतव्य में सफल है। कथाक्रम में पात्रों की बुनावट बहुत सलीके से की गई है। यह कहानी पहले कहां छपी, उल्लेख नहीं है।
” शहादत ” भी आंचलिक है। मुख्य पात्र फ़ौजी काका हैं, जिनके सीमा पर युद्ध में बाएं पैर में गोली लगी थी। गांव में रहते हैं और गंवाई सियासत का शिकार होकर वीरगति को प्राप्त हुए। नवविर्वाचित प्रधान के विरोध का उन्हें कुफल भोगना पड़ा। वे सत्य पर थे और गांव में स्कूल बनवाने के लिए प्रयासरत थे। प्रस्तावित भूमि पर प्रधान की नज़र टिकी और वह उसके व्यावसायिक इस्तेमाल की दिशा में आगे बढ़ा,तो फ़ौजी काका ने विरोध किया, तो दरवाजे पर मौत खड़ी मिली। धारदार हथियारों से उन पर हमला किया गया। वे बच नहीं सके। पाठशाला मधुशाला बन गई। फ़ौजी काका के एक – दो डायलाग बड़े धारदार हैं, यथा –
” पहले के लोग डॉक्टर को भगवान कहते थे, पर आज का डॉक्टर ख़ुद को भगवान समझता है।”
” सैनिकों को पेंशन और कुछ रियायतें सरकार देती है, तो कोई एहसान नहीं करती।”
लेकिन काका का यह संवाद युग दृष्टि के लिहाज़ से अनुकूल नहीं –
” मैं कैसे समझाऊं इस कम बुद्धि औरत को। यह चाहती है कि मैं रामदीन के बैलों को जलकर मर जाने देता।”
यह कहानी अपने उद्देश्य में एकदम सफल है। प्रस्तुतीकरण स्तरीय है। आजकल ग्रामीणांचल में इस प्रकार की ओछी हरकतें सहज सुलभ हैं।
” कंक्रीट के जंगल में ” भौतिकवाद और तथाकथित आधुनिकवाद पर चोट करने में सक्षम है। वर्तमान में बेटे/ बेटों द्वारा माता – पिता की घोर उपेक्षा का आलम है। वे अपने स्वार्थ में इतने डूब चुके हैं कि उनकी देखरेख से आम तौर से अपने को दूर कर रखा है। वे उनके भी किसी काम नहीं आते, जिन्होंने उनकी परवरिश की है। मां के भी नहीं, जिनके उपकारों की इंतिहा नहीं ! ऐसी ही भ्रष्ट मानसिकता की प्रतिबिंब है यह कहानी। पूरी तरह मनोवैज्ञानिक है, जो गहरे मानसिक परिवर्तन का विवेचन करती है।
” मजमा ” और ” गुनहगार ” दोनों कथाओं की पृष्ठभूमि राजनीतिक हैं। राजनेताओं के दोहरे चरित्र को बखूबी उजागर करने में कामयाब हैं। जनता के साथ सही तौर पर जुड़ना और उनका सुख – दुख जानकर आवश्यकतानुसार सहयोग करना हमारे नेताओं को आया ही नहीं। बस वोट का मतलब निकल जाए, तो पहचानते नहीं। ” मजमा ” में तो नेताजी के भाषण के तत्काल बाद जनता के साथ अपमान का खेल शुरू हो जाता है। यह कहानी बलरामपुर के वीर विनय चौक के इर्द – गिर्द घूमती है। वीर विनय कायस्थ देश के महान सैनिकों में से थे। यहां चौक पर उनकी प्रतिमा स्थापित है। तब नहीं स्थापित थी, जब यह कहानी रची गई। फरवरी 2009 में यह कहानी लिखी गई। उस समय की स्थिति को बयान करते हुए रचनाकार ने इस कहानी में लिखा है, ” शहर की सामाजिक संस्था ” पैगाम ” के संयोजक श्री आज़ाद सिंह और उनके उनके कई बुद्धिजीवी सहयोगी पिछले कई बरसों से यहां शहीद विनय की प्रतिमा स्थापना के लिए युद्ध स्तरीय प्रयास कर रहे हैं। पर गनीमत है, अभी तक ऐसा नहीं हो पाया।”
वीर विनय कायस्थ लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में अपनी प्रतिमा में हैं ! रचनाकार ढहते लोकतंत्र पर प्रतिमा की आंखों से आंसू निकलने की कल्पना यूं हीं नहीं करता, बल्कि उसे यकीन है कि अमर शहीद की प्रतिमा अवश्य लगेगी। हुआ भी ऐसा ही। कथा प्रकाशन के बाद प्रतिमा लग गई, जो लोकतंत्र की संरक्षा की याद दिलाती रहेगी सदा। कथाकार के शब्दों में ” लोकतंत्र के नाम पर बार – बार ठगे जाते निरीह देशवासियों को देख अमर शहीद की पत्थर की आंखों में भी आंसू आ जाते …।”
“गुनहगार” में राजनेताओं का दर्शन समझने की जनता की कोशिश की चर्चा भी है। एक बालक भी समझने को व्यग्र होता है।अपनी साइकिल की परवाह न कर नेताजी को देखने – समझने के लिए चल पड़ता है, लेकिन साइकिल से हाथ धो बैठता है। वह साइकिल भी उसकी न थी। अब घर में मम्मी मारेंगी, यह सोचकर चिंतित हो उठता है। सिपाही राम प्रसाद को जब यह पता चलता है, तो वह बालक को दूसरी साइकिल चोरुआ देता है। आगे चलकर बालक प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है और सिपाही प्रमोट होकर एस आई टी में चला जाता है। सिपाही इतना उदारमना है कि उसका दिल बालक को गुनहगार मानने को तैयार नहीं ! इस कथा का संदेश गुंजलक है, फिर भी रोचक है। सियासतदानों गिरगिटी किरदार पर तंज़ है, जो कथाकार के इन शब्दों में व्यक्त होता है –
” यहां के आम शहरी में अब चुनावी रैलियों को लेकर ज़रा भी उत्साह नहीं दिखता। इसकी वजह संभवतः यही है कि राजनीतिज्ञ अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं और उनकी कथनी – करनी के फ़र्क को सब बखूबी समझ चुके हैं।” ( पृष्ठ 80 )
” मंडी ” दरकते पारिवारिक रिश्तों की कथा है। अपना ही पुत्र उच्च पद पर पहुंचते ही किस प्रकार पिता, भाई, भाभी और भतीजों की उपेक्षा करता है और अपने रुतबे में रहता है, इसका अच्छा चित्रण इस कथा में है। इसका मंतव्य, संरचना और गठन उल्लेखनीय है। स्वान कथा ” पागल ” दमदार है। रचनाकार ने इसमें विचारणीय प्रश्न उठाए हैं। कुत्ते को मार डालने वाला इन्सान पागल था या कुत्ता ? यह पशु जीवन अधिकार की वकालत करती हुई बेजोड़ कहानी है। ” दूसरा बिछोह ” भी आंचलिक है, लेकिन संवेदनाओं से लबरेज़ के साथ बड़ी मार्मिक है। कर्म से शर्मसार होकर रूपा की आत्महत्या बहुत कुछ सोचने पर विवश कर देती है। परिस्थितियों की मार से पारस को पति से साधु बनना पड़ा। कथाकर यदि रूपा की आत्महत्या न दिखाकर कोई और ट्रेजेडी दिखाता, तो और बेहतर होता।
आज के युग में मित्र भी स्वार्थी हो गए हैं। वे एहसान तक भूल जाते हैं। इसका खुलासा करती है कहानी ” मित्र – ऋण ” जो लघुकथा भी भांति शीघ्र समाप्त हो जाती है। जबकि अंतिम कहानी ” कस्बाई लड़की की प्रेम कथा ” लंबी चलती है, अंतर्जातीय विवाह की दुश्वारियों को बयान करती हुई। दुखांत ही इसका समान्य परिणाम आता है, जो कथा में भी आया। इस कथा का प्रबोधन साफ़ है, ” विश्वास की दीवार ऐसी ही होती है, जल्द ढहती नहीं, पर जब गिरती है, तो भारभरा कर गिरती है। फिर वहां कुछ भी नहीं बचता , स्मृतियों के गुबार के सिवा।” ( पृष्ठ 112 )
112 पृष्ठों की इस पुस्तक में प्रूफ की कुछ गलतियां हैं। छपाई सुंदर है। प्वाइंट साइज़ कुछ बड़ा होता , तो और अच्छा होता। पृष्ठों को अनावश्यक रिड्यूस किया गया है, जो ठीक नहीं लगता। रिड्यूस कम किया जाता, तो प्वाइंट साइज़ ठीक रहता।
समदर्शी प्रकाशन, मेरठ से छपी इस पुस्तक की भूमिका कैलाश बनवासी ने लिखी है। भूमिका भी समीक्षा की तरह है। रचनाकार और संबद्ध महानुभावों को अंतर्मन से बधाई !
– Dr RP Srivastava, Editor – in – Chief , ” Bharatiya Sanvad “